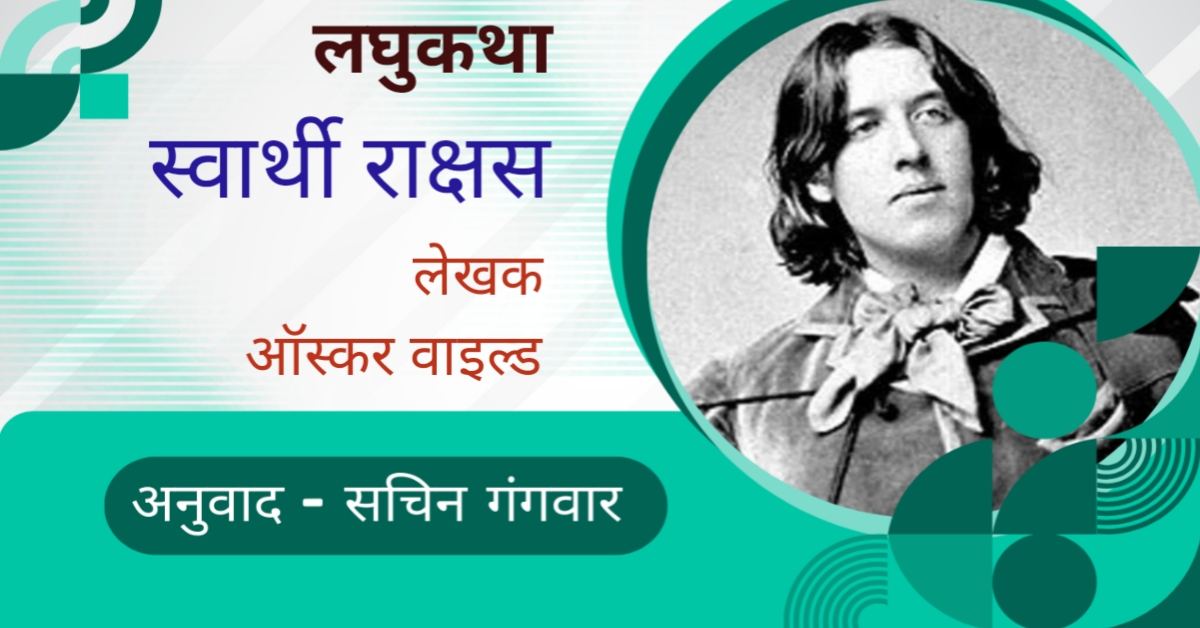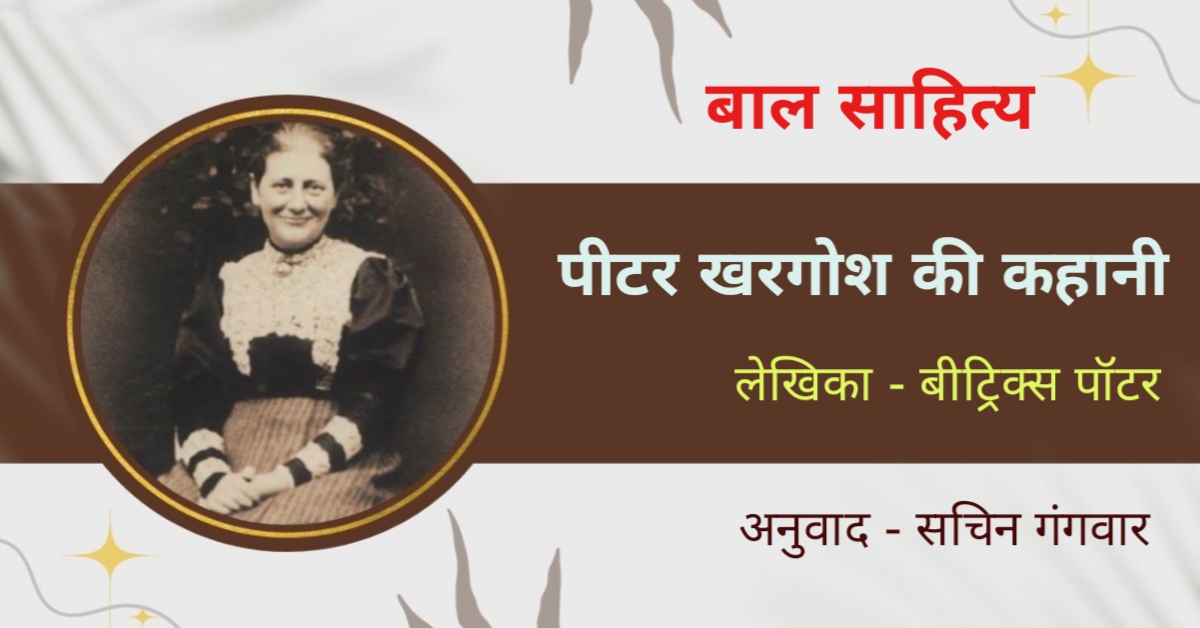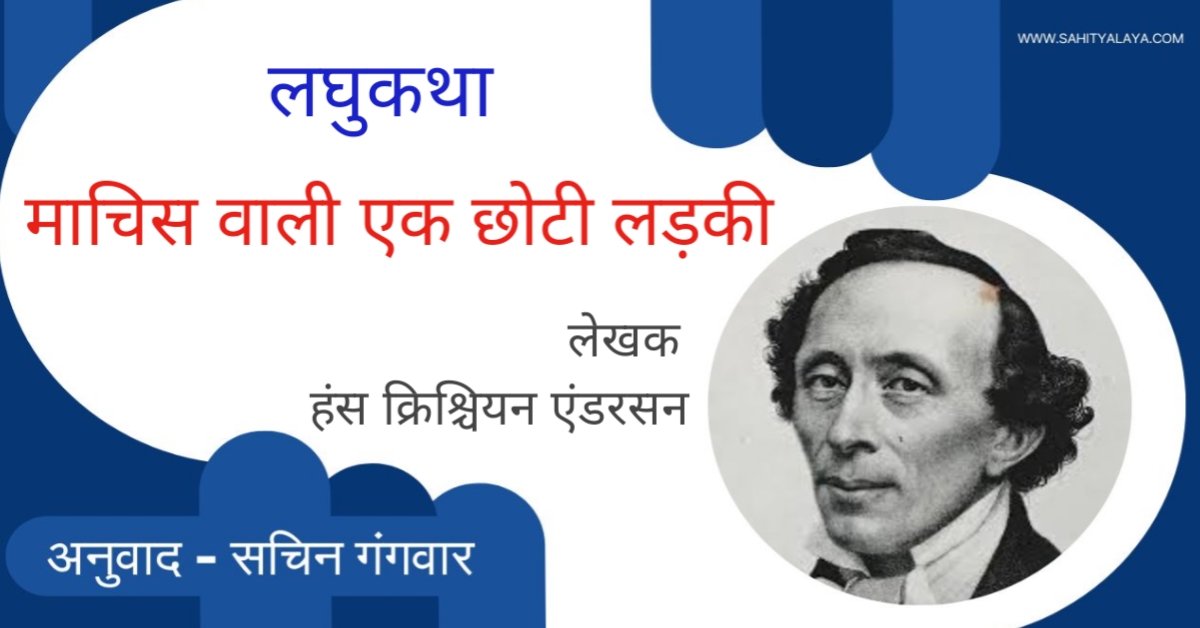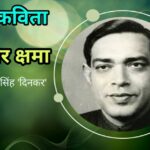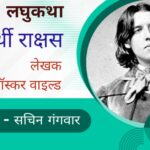ले दे के अपने पास फ़क़त इक नज़र तो है
क्यूं देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम
साहिर लुधियानवी
Sahityalaya
एक दिन धधको नहीं, तिल-तिल जलो,
नित्य कुछ मिटते हुए बढ़ते चलो।
पूर्णता पर आ चुका जब नाश हो,
जान लो, आराध्य के तुम पास हो।
(रामधारी सिंह ‘दिनकर’)